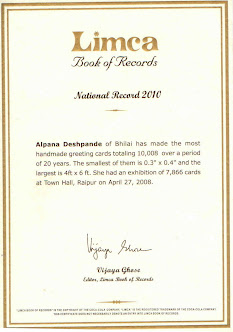बिगड़ता मिजाज मौसम का----योगेश कुमार गोयल
>> रविवार, 20 फ़रवरी 2011
योगेश कुमार गोयल
 समाचार-फीचर एजेंसियों ‘मीडिया केयर नेटवर्क’, ‘मीडिया एंटरटेनमेंट फीचर्स’ तथा ‘मीडिया केयर न्यूज’ में प्रधान सम्पादक। राजनीतिक, सामयिक तथा सामाजिक विषयों पर विश्लेषणात्मक लेख, रिपोर्ट व सृजनात्मक लेखन। दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक ट्रिब्यून, स्वतंत्र वार्ता, राजस्थान पत्रिका, नवभारत, लोकमत समाचार, रांची एक्सप्रेस, अजीत समाचार, पा×चजन्य, कादम्बिनी, शुक्रवार, सरिता, मुक्ता, सरस सलिल, विचार सारांश, इंडिया न्यूज इत्यादि अनेक प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में विगत 20 वर्षों में विभिन्न विषयों पर 8500 से अधिक लेख, रिपोर्ट, फीचर इत्यादि प्रकाशित। आकाशवाणी रोहतक से दो दर्जन विशेष वार्ताएं प्रसारित। नशे के दुष्प्रभावों पर 1993 में ‘मौत को खुला निमंत्रण’ पुस्तक (पांच विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत), ‘हरियाणा साहित्य अकादमी’ के सौजन्य से 2009 में ‘जीव-जंतुओं की अनोखी दुनिया’ पुस्तक तथा 2009 में ‘तीखे तेवर’ पुस्तक प्रकाशित। पत्रकारिता व साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जिला प्रशासन रोहतक, वाईएमसीए इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, भारतीय दलित साहित्य अकादमी, विंध्यवासिनी जनकल्याण ट्रस्ट, अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा विकास संगठन, अखिल भारतीय साहित्य कला मंच, अनुराग सेवा संस्थान इत्यादि अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित।
समाचार-फीचर एजेंसियों ‘मीडिया केयर नेटवर्क’, ‘मीडिया एंटरटेनमेंट फीचर्स’ तथा ‘मीडिया केयर न्यूज’ में प्रधान सम्पादक। राजनीतिक, सामयिक तथा सामाजिक विषयों पर विश्लेषणात्मक लेख, रिपोर्ट व सृजनात्मक लेखन। दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक ट्रिब्यून, स्वतंत्र वार्ता, राजस्थान पत्रिका, नवभारत, लोकमत समाचार, रांची एक्सप्रेस, अजीत समाचार, पा×चजन्य, कादम्बिनी, शुक्रवार, सरिता, मुक्ता, सरस सलिल, विचार सारांश, इंडिया न्यूज इत्यादि अनेक प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में विगत 20 वर्षों में विभिन्न विषयों पर 8500 से अधिक लेख, रिपोर्ट, फीचर इत्यादि प्रकाशित। आकाशवाणी रोहतक से दो दर्जन विशेष वार्ताएं प्रसारित। नशे के दुष्प्रभावों पर 1993 में ‘मौत को खुला निमंत्रण’ पुस्तक (पांच विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत), ‘हरियाणा साहित्य अकादमी’ के सौजन्य से 2009 में ‘जीव-जंतुओं की अनोखी दुनिया’ पुस्तक तथा 2009 में ‘तीखे तेवर’ पुस्तक प्रकाशित। पत्रकारिता व साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जिला प्रशासन रोहतक, वाईएमसीए इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, भारतीय दलित साहित्य अकादमी, विंध्यवासिनी जनकल्याण ट्रस्ट, अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा विकास संगठन, अखिल भारतीय साहित्य कला मंच, अनुराग सेवा संस्थान इत्यादि अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित।सम्पर्क: मीडिया केयर ग्रुप, मेन बाजार बादली, जिला झज्जर (हरियाणा)-124105
पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज न केवल भारत में बल्कि विश्वभर में चिन्ता निरन्तर गहरा रही है। दरअसल मौसम की मार अब किसी खास महीने में अथवा किसी खास देश पर देखने को नहीं मिल रही बल्कि मौसम की यह मार हर जगह, हर कहीं साल दर साल लगातार बढ़ रही है बल्कि अब तो ऐसा लगने लगा है, जैसे हर मौसम अपनी मारक क्षमता दिखाने के लिए ही आता है। गर्मी में जहां पारा 47-48 डिग्री तक जा पहुंचता है, वहीं सर्दियों में यह अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में भी लोगों को बुरी तरह कंपकंपा जाता है और बरसात में कहीं इस कदर बारिश होती है कि लोग बाढ़ की विभीषिका झेलने को विवश हो जाएं तो कहीं लोग वर्षा ऋतु में भी एक-एक बूंद पानी को तरसते दिखाई पड़ते हैं और अकाल की नौबत आ जाती है।
कुछ वर्ष पूर्व जनवरी माह के शुरू में खासतौर से उत्तर भारत में मौसम ने जो सितम ढ़ाया था, उससे हर कोई हतप्रभ था। तब दिल्ली में जहां पारे ने 0.2 डिग्री पर पहुंचकर 70 साल का रिकार्ड ध्वस्त कर दिया था, वहीं कश्मीर की डल झील इस कदर जम गई थी कि लोगों ने उस पर जमकर क्रिकेट खेला, कुछ अन्य हिस्सों में पारा शून्य डिग्री से भी नीचे पहुंच गया था तो ठंडी जगह माने जाने वाले शिमला में उसी दौरान तापमान छह डिग्री दर्ज किया गया था। तब एक ओर जहां एकाएक बढ़ी ठंड ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर जान-माल को काफी नुकसान पहुंचाया था, वहीं जनवरी के दूसरे पखवाड़े में मौसम बहुत काफी गर्म रहा था। इसे मौसम का बिगड़ता मिजाज नहीं तो और क्या माना जाए?
अमेरिका में कैटरीना और रीटा नामक तूफानों के चलते हुई भयानक तबाही, भारतीय उपमहाद्वीप में आया विनाशकारी भूकम्प, भारत में इस वर्ष कई राज्यों में आई भयानक बाढ़, क्या इन्हें भी प्रकृति का प्रकोप ही नहीं माना जाएगा? अंटार्कटिका में पिघलती बर्फ और वहां उगती घास ने भी सबको हैरत में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लेकिन यह सब हमारे दुष्कृत्यों का ही नतीजा है क्योंकि प्रकृति से हमारी छेड़छाड़ जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है तथा पर्यावरण संतुलन को हमने बुरी तरह बिगाड़ दिया है। हमारी लापरवाहियों का ही नतीजा है कि भूगर्भीय जल भी अब दूषित होने लगा है और बढ़ते प्रदूषण के चलते जहरीली गैसें ‘एसिड’ की बरसात करने लगी हैं।
पृथ्वी का निरन्तर बढ़ता तापमान और जलवायु में लगातार हो रहे भारी बदलाव आज किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि समूचे विश्व में मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। मौसम का बिगड़ता मिजाज मानव जाति, जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों के लिए तो बहुत खतरनाक है ही, पर्यावरण संतुलन के लिए भी एक गंभीर खतरा है। हालांकि प्रकृति बार-बार अपने प्रकोप, अपनी प्रचंडता के जरिये हमें इस ओर से सावधान करने की भरसक कोशिश भी करती है पर हम हैं कि लगातार इन खतरों की अनदेखी किए जा रहे हैं। पर्यावरण का संतुलन जिस कदर बिगड़ रहा है, ऐसे में जरूरत इस बात की है कि बचपन से ही हमें पर्यावरण की हानि से होने वाली गंभीर समस्याओं के बारे में सचेत किया जाए और यह सिखाया जाए कि हम अपने-अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में या भागीदारी निभा सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 10 हजार वर्षों में भी पृथ्वी पर जलवायु में इतना बदलाव और तापमान में इतनी बढ़ोतरी नहीं देखी गई, जितनी हाल के कुछ ही वर्षों में देखी गई है। मौसम के इस बदलते मिजाज के लिए औद्योगिकीकरण, बढ़ती आबादी, घटते वनक्षेत्र, वाहनों के बढ़ते कारवां तथा तेजी से बदलती जीवनशैली को खासतौर से जिम्मेदार माना जा सकता है। ‘ग्लोबल वार्मिंग’ की विकराल होती समस्या के लिए औद्योगिक इकाईयों और वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, जिनका वायुमंडल में उत्सर्जन विश्वभर में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति के बाद से काफी तेजी से बढ़ा है।
पृथ्वी तथा इसके आसपास के वायुमंडल का तापमान सूर्य की किरणों के प्रभाव अथवा तेज से बढ़ता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने के बाद इनकी अतिरिक्त गर्मी वायुमंडल में मौजूद धूल के कणों एवं बादलों से परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। इस प्रकार पृथ्वी के तापमान का संतुलन बरकरार रहता है लेकिन कुछ वर्षों से वायुमंडल में हानिकारक गैसों का जमावड़ा बढ़ते जाने और इन गैसों की वायुमंडल में एक परत बन जाने की वजह से पृथ्वी के तापमान का संतुलन निरन्तर बिगड़ रहा है। दरअसल हानिकारक गैसों की इस परत को पार करके सूर्य की किरणें पृथ्वी तक तो आसानी से पहुंच जाती हैं लेकिन यह परत उन किरणों के वापस लौटने में बाधक बनती है और यही पृथ्वी का तापमान बढ़ते जाने का मुख्य कारण है।
जिस प्रकार वनस्पतियों के लिए (पौधों के शीघ्र विकास के लिए) बनाया जाने वाला ‘ग्रीन हाउस’ (शीशे का घर) सूर्य की ऊर्जा को इस ग्रीन हाउस के अंदर तो आने देता है लेकिन ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता और परिणामतः ग्रीन हाउस के भीतर का तापमान काफी बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार वायुमंडल में विभिन्न जहरीली गैसों की एक परत बन जाने से वह परत भी इस ग्रीन हाउस की भांति सूर्य की गर्मी को परत को पार करके पृथ्वी तक जाने तो देती है लेकिन वापस नहीं लौटने देती। इसी वजह से इस प्रक्रिया को ‘ग्रीन हाउस इफैक्ट’ कहा जाता है और हानिकारक गैसों की इस परत को ‘ग्रीन हाउस लेयर’ तथा इस परत के निर्माण में सक्रिय गैसों को ‘ग्रीन हाउस गैस’ कहा जाता है।
मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों में ‘क्लोरो फ्लोरो कार्बन’ परिवार की गैसें शामिल हैं, जो औद्योगिक इकाईयों में बड़ी मात्रा में उपयोग की जाती हैं। इन गैसों में कोयले, पैट्रोल, डीजल, तेल, जीवाश्म ईंधन आदि से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक खतरनाक ‘ग्रीन हाउस गैस’ मानी जाती है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार 1960 के बाद से ही वायुमंडल में इस गैस की मात्रा में 25 फीसदी वृद्धि हुई है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ते जाने के साथ-साथ ज्यों-ज्यों वायमुंडल में ग्रीन हाउस लेयर की मोटाई बढ़ती जा रही है, पृथ्वी का तापमान भी उसी के अनुरूप लगातार बढ़ रहा है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पिछली सदी के दौरान वर्ष दर वर्ष पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा और पिछली सदी का अंतिम दशक तो विगत 1000 से भी अधिक वर्षों के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म रहा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पृथ्वी के इतिहास में कोई भी जलवायु परिवर्तन इतनी तीव्र गति से नहीं हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी 50 वर्षों तक पर्यावरण प्रदूषण और पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी की यही गति जारी रही तो इस सदी के मध्य तक इस तापमान में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो सकती है और ऐसा हुआ तो ‘महाप्रलय’ की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार सन् 2050 तक पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की संभावना है।
इसलिए यदि समय रहते ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडल में उत्सर्जन पर अंकुश न लगाया गया तो आने वाले वर्षों में इसके बहुत विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। इससे विश्व भर में मौसम का संतुलन बुरी तरह डगमगा जाएगा और ऋतुओं का आपसी संतुलन बिगड़ जाने से एक प्रकार से महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पृथ्वी पर वायुमंडल का तापमान निरन्तर बढ़ते जाने से हिमशिखर पिघलते जाएंगे और इस तरह बर्फ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तथा समुद्र तल ऊंचे उठने व जलस्तर बढ़ने के कारण एक ओर जहां समुद्रों के किनारे बसे अनेक शहर जलमग्न हो जाएंगे, वहीं बाढ़ की विभीषिका भी उत्पन्न होगी तथा कृषि योग्य भूमि निरन्तर घटती जाएगी। इस प्रकार दुनिया भर में अकाल जैसी भयानक समस्या के सिर उठाने से करोड़ों लोग भूखे मरने के कगार पर पहुंच जाएंगे।
बहरहाल, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जिस प्रकार निरन्तर विकराल होती जा रही है और मौसम के इस बदलते मिजाज का खामियाजा भी चूंकि विकसित देशों के बजाय विकासशील देशों को ही अधिक भुगतना पड़ता है, अतः विकासशील देशों को चाहिए कि वे अमेरिका सरीखे विकसित देश पर इस बात के लिए दबाव बनाएं कि वह प्रकृति के विरूद्ध अपनी छेड़छाड़ बंद कर पर्यावरण सुधार की मुहिम में अपना भी महत्वपूर्ण योगदान दे।
योगेश कुमार गोयलकुछ वर्ष पूर्व जनवरी माह के शुरू में खासतौर से उत्तर भारत में मौसम ने जो सितम ढ़ाया था, उससे हर कोई हतप्रभ था। तब दिल्ली में जहां पारे ने 0.2 डिग्री पर पहुंचकर 70 साल का रिकार्ड ध्वस्त कर दिया था, वहीं कश्मीर की डल झील इस कदर जम गई थी कि लोगों ने उस पर जमकर क्रिकेट खेला, कुछ अन्य हिस्सों में पारा शून्य डिग्री से भी नीचे पहुंच गया था तो ठंडी जगह माने जाने वाले शिमला में उसी दौरान तापमान छह डिग्री दर्ज किया गया था। तब एक ओर जहां एकाएक बढ़ी ठंड ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर जान-माल को काफी नुकसान पहुंचाया था, वहीं जनवरी के दूसरे पखवाड़े में मौसम बहुत काफी गर्म रहा था। इसे मौसम का बिगड़ता मिजाज नहीं तो और क्या माना जाए?
अमेरिका में कैटरीना और रीटा नामक तूफानों के चलते हुई भयानक तबाही, भारतीय उपमहाद्वीप में आया विनाशकारी भूकम्प, भारत में इस वर्ष कई राज्यों में आई भयानक बाढ़, क्या इन्हें भी प्रकृति का प्रकोप ही नहीं माना जाएगा? अंटार्कटिका में पिघलती बर्फ और वहां उगती घास ने भी सबको हैरत में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लेकिन यह सब हमारे दुष्कृत्यों का ही नतीजा है क्योंकि प्रकृति से हमारी छेड़छाड़ जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है तथा पर्यावरण संतुलन को हमने बुरी तरह बिगाड़ दिया है। हमारी लापरवाहियों का ही नतीजा है कि भूगर्भीय जल भी अब दूषित होने लगा है और बढ़ते प्रदूषण के चलते जहरीली गैसें ‘एसिड’ की बरसात करने लगी हैं।
पृथ्वी का निरन्तर बढ़ता तापमान और जलवायु में लगातार हो रहे भारी बदलाव आज किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि समूचे विश्व में मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। मौसम का बिगड़ता मिजाज मानव जाति, जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों के लिए तो बहुत खतरनाक है ही, पर्यावरण संतुलन के लिए भी एक गंभीर खतरा है। हालांकि प्रकृति बार-बार अपने प्रकोप, अपनी प्रचंडता के जरिये हमें इस ओर से सावधान करने की भरसक कोशिश भी करती है पर हम हैं कि लगातार इन खतरों की अनदेखी किए जा रहे हैं। पर्यावरण का संतुलन जिस कदर बिगड़ रहा है, ऐसे में जरूरत इस बात की है कि बचपन से ही हमें पर्यावरण की हानि से होने वाली गंभीर समस्याओं के बारे में सचेत किया जाए और यह सिखाया जाए कि हम अपने-अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में या भागीदारी निभा सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 10 हजार वर्षों में भी पृथ्वी पर जलवायु में इतना बदलाव और तापमान में इतनी बढ़ोतरी नहीं देखी गई, जितनी हाल के कुछ ही वर्षों में देखी गई है। मौसम के इस बदलते मिजाज के लिए औद्योगिकीकरण, बढ़ती आबादी, घटते वनक्षेत्र, वाहनों के बढ़ते कारवां तथा तेजी से बदलती जीवनशैली को खासतौर से जिम्मेदार माना जा सकता है। ‘ग्लोबल वार्मिंग’ की विकराल होती समस्या के लिए औद्योगिक इकाईयों और वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, जिनका वायुमंडल में उत्सर्जन विश्वभर में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति के बाद से काफी तेजी से बढ़ा है।
पृथ्वी तथा इसके आसपास के वायुमंडल का तापमान सूर्य की किरणों के प्रभाव अथवा तेज से बढ़ता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने के बाद इनकी अतिरिक्त गर्मी वायुमंडल में मौजूद धूल के कणों एवं बादलों से परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। इस प्रकार पृथ्वी के तापमान का संतुलन बरकरार रहता है लेकिन कुछ वर्षों से वायुमंडल में हानिकारक गैसों का जमावड़ा बढ़ते जाने और इन गैसों की वायुमंडल में एक परत बन जाने की वजह से पृथ्वी के तापमान का संतुलन निरन्तर बिगड़ रहा है। दरअसल हानिकारक गैसों की इस परत को पार करके सूर्य की किरणें पृथ्वी तक तो आसानी से पहुंच जाती हैं लेकिन यह परत उन किरणों के वापस लौटने में बाधक बनती है और यही पृथ्वी का तापमान बढ़ते जाने का मुख्य कारण है।
जिस प्रकार वनस्पतियों के लिए (पौधों के शीघ्र विकास के लिए) बनाया जाने वाला ‘ग्रीन हाउस’ (शीशे का घर) सूर्य की ऊर्जा को इस ग्रीन हाउस के अंदर तो आने देता है लेकिन ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता और परिणामतः ग्रीन हाउस के भीतर का तापमान काफी बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार वायुमंडल में विभिन्न जहरीली गैसों की एक परत बन जाने से वह परत भी इस ग्रीन हाउस की भांति सूर्य की गर्मी को परत को पार करके पृथ्वी तक जाने तो देती है लेकिन वापस नहीं लौटने देती। इसी वजह से इस प्रक्रिया को ‘ग्रीन हाउस इफैक्ट’ कहा जाता है और हानिकारक गैसों की इस परत को ‘ग्रीन हाउस लेयर’ तथा इस परत के निर्माण में सक्रिय गैसों को ‘ग्रीन हाउस गैस’ कहा जाता है।
मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों में ‘क्लोरो फ्लोरो कार्बन’ परिवार की गैसें शामिल हैं, जो औद्योगिक इकाईयों में बड़ी मात्रा में उपयोग की जाती हैं। इन गैसों में कोयले, पैट्रोल, डीजल, तेल, जीवाश्म ईंधन आदि से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक खतरनाक ‘ग्रीन हाउस गैस’ मानी जाती है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार 1960 के बाद से ही वायुमंडल में इस गैस की मात्रा में 25 फीसदी वृद्धि हुई है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ते जाने के साथ-साथ ज्यों-ज्यों वायमुंडल में ग्रीन हाउस लेयर की मोटाई बढ़ती जा रही है, पृथ्वी का तापमान भी उसी के अनुरूप लगातार बढ़ रहा है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पिछली सदी के दौरान वर्ष दर वर्ष पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा और पिछली सदी का अंतिम दशक तो विगत 1000 से भी अधिक वर्षों के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म रहा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पृथ्वी के इतिहास में कोई भी जलवायु परिवर्तन इतनी तीव्र गति से नहीं हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी 50 वर्षों तक पर्यावरण प्रदूषण और पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी की यही गति जारी रही तो इस सदी के मध्य तक इस तापमान में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो सकती है और ऐसा हुआ तो ‘महाप्रलय’ की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार सन् 2050 तक पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की संभावना है।
इसलिए यदि समय रहते ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडल में उत्सर्जन पर अंकुश न लगाया गया तो आने वाले वर्षों में इसके बहुत विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। इससे विश्व भर में मौसम का संतुलन बुरी तरह डगमगा जाएगा और ऋतुओं का आपसी संतुलन बिगड़ जाने से एक प्रकार से महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पृथ्वी पर वायुमंडल का तापमान निरन्तर बढ़ते जाने से हिमशिखर पिघलते जाएंगे और इस तरह बर्फ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तथा समुद्र तल ऊंचे उठने व जलस्तर बढ़ने के कारण एक ओर जहां समुद्रों के किनारे बसे अनेक शहर जलमग्न हो जाएंगे, वहीं बाढ़ की विभीषिका भी उत्पन्न होगी तथा कृषि योग्य भूमि निरन्तर घटती जाएगी। इस प्रकार दुनिया भर में अकाल जैसी भयानक समस्या के सिर उठाने से करोड़ों लोग भूखे मरने के कगार पर पहुंच जाएंगे।
बहरहाल, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जिस प्रकार निरन्तर विकराल होती जा रही है और मौसम के इस बदलते मिजाज का खामियाजा भी चूंकि विकसित देशों के बजाय विकासशील देशों को ही अधिक भुगतना पड़ता है, अतः विकासशील देशों को चाहिए कि वे अमेरिका सरीखे विकसित देश पर इस बात के लिए दबाव बनाएं कि वह प्रकृति के विरूद्ध अपनी छेड़छाड़ बंद कर पर्यावरण सुधार की मुहिम में अपना भी महत्वपूर्ण योगदान दे।