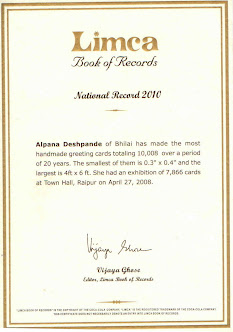दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
आज पर्यावरण की हानि होने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से पूरी दुनिया को जुझना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान सामने आ रहे हैं। हम पर्यावरण की रक्षा करें एवं आने वाली पी्ढी के लिए स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें। पर्यावरण के प्रति जागरुक करने के लिए हम एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं।प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए सूचना एवं नियम इस प्रकार है।
विषय -- "बचपन और हमारा पर्यावरण"
प्रथम पुरस्कार
11000/= (ग्यारह हजार रुपए नगद)
एवं प्रमाण-पत्र
द्वितीय पुरस्कार
5100/= (इक्यावन सौ रुपए नगद)
एवं प्रमाण-पत्र
तृती्य पुरस्कार
2100/= (इक्की्स सौ रुपए नगद)
एवं प्रमाण-पत्र
सांत्वना पुरस्कार (10)
501/=(पाँच सौ एक रुपए नगद)
एवं प्रमाण-पत्र
1. इस प्रतियोगिता में 1 नवम्बर 2010 से 30 नवंबर 2010 तक आलेख भेजे जा सकते है.
2. प्रतियोगिता में सिर्फ़ दिए गए विषय पर ही आलेख सम्मिलित किए जाएंगे।
3. एक रचनाकार अपने अधिकतम 3 अप्रकाशित मौलिक आलेख भेज सकता है पुरस्कृत होने की स्थिति में वह केवल एक ही पुरस्कार का हकदार होगा.
4. स्व रचित आलेख 1 नवम्बर 2010 से 30 नवंबर 2010 तक lekhcontest@gmail.com पर भेज सकते हैं. कृपया साथ में मौलिकता का प्रमाण-पत्र एवं अपना एक अधिकतम १०० शब्दों में परिचय तथा तस्वीर भी संलग्न करें। नियमावली की कंडिका 7 से संबंध नहीं होने का का भी उल्लेख प्रमाण-पत्र में करें। आलेख कम से कम 500 एवं अधिकतम 1000 शब्दों में होने चाहिए।
आपसे निवेदन है कि प्रत्येक रचना को अलग अलग इमेल से भेजने की कृपा करें. यानि एक इमेल से एक बार मे एक ही रचना भेजे.
5. हमें प्राप्त रचनाओं मे से जो भी रचना प्रतियोगिता में शामिल होने लायक पायी जायेगी उसे हमारे सहयोगी ब्लाग
"हमारा पर्यावरण" पर प्रकाशित कर दिया जायेगा, जो इस बात की सूचना होगी कि प्रकाशित रचना प्रतियोगिता में शामिल कर ली गई है।
6. 1 दिसंबर 2010 से प्रतियोगिता में सम्मिलित आलेखों का प्रकाशन
"हमारा पर्यावरण" पर प्रारंभ कर दिया जायेगा.
7. इस प्रतियोगिता में हमारा पर्यावरण, एसार्ड, एवं पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित कोई भी व्यक्ति या उसका करीबी रिश्तेदार भाग लेने की पात्रता नहीं रखता।
8. इन रचनाओं पर
"हमारा पर्यावरण" का कापीराईट रहेगा. और कहीं भी उपयोग और प्रकाशन का अधिकार हमें होगा.
9. रचनाओं को पुरस्कृत करने का अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ़
"हमारा पर्यावरण" के संचालकों के पास सुरक्षित रहेगा. इस विषय मे किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार नही किया जायेगा और ना ही किसी को कोई जवाब दिया जायेगा.
10. इस प्रतियोगिता के समस्त अधिकार और निर्णय के अधिकार सिर्फ़
"हमारा पर्यावरण" के पास सुरक्षित हैं. प्रतियोगिता के नियम किसी भी स्तर पर परिवर्तनीय है.
11.पुरस्कार
IASRD द्वारा प्रायोजित हैं.
12. यह प्रतियोगिता पर्यावरण के प्रति जागरुकता लाने के लिए एवं हिंदी मे स्वस्थ लेखन को बढावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है.
(नोट:-प्रतियोगिता में ब्लॉग जगत के अलावा अन्य भी भाग ले सकते हैं प्रतियोगी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए)
Read more...